बलराम शुक्ल द्वारा
सूत्राम्भसं पदावर्तं पारायणरसातलम् । धातूणादिगणग्राहं ध्यानग्रहबृहत्प्लवम्
धीरैरालोकितप्रान्तं अमेधोभिरसूयितम् । सदोपभुक्तं सर्वाभिरन्यविद्याकरेणुभिः ॥
नापारयित्वा दुर्गाधममुं व्याकरणार्णवम्। शब्दरत्नं स्वयंगम्यम् अलं कर्तुमयं जनम्[2] ॥
भारतीय ज्ञान परम्परा में असंख्य विद्वानों की शृंखला के मध्य अनेक महान् विद्वान् प्रकाश स्तम्भ की भाँति विद्यमान हैं जिनकी आभा, सहस्राब्दियों का समय बीत जाने के बाद भी; उनके स्थानों में आमूलचूल सामाजिक परिवर्तन हो जाने के बावजूद, मन्द नहीं पड़ सकी है। महर्षि वेदव्यास, आचार्य पाणिनि तथा भगवान् शंकराचार्य के साथ महामाहेश्वर अभिनवगुप्तपादाचार्य ऐसे ही महापुरुषों में से एक हैं। आचार्य पाणिनि सीमान्त प्रान्त के शलातुर ग्राम (सम्भवतः आधुनिक लाहौर) के निवासी थे। उन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की जो भारत की सांस्कृतिक एकता की मूल भाषा संस्कृत को ठीक ठीक समझने में हजारों साल तक उपयुक्त होती रही है। लाहौर अब हमारे पास नहीं है लेकिन अष्टाध्यायी अब भी हमें अपनी सांस्कृतिक निधि को सुरक्षित करने में निरन्तर सहयोग कर रही है। अभिनव गुप्त आज से लगभग एक हजार वर्ष पहले कश्मीर में वर्तमान थे। उन्होंने अद्वैत दर्शन के जिस काश्मीर संस्करण का व्याख्यान किया वह भारत की दार्शनिक स्मृति में अमिट है। उनके द्वारा काव्यशास्त्रीय सिद्धान्तों के बारे दी गयी व्याख्यायें आज तक अन्तिम मानी जा रही हैं। आज शारदादेश कश्मीर का पर्याय नहीं है। भारत की अखण्ड सांस्कृतिक भावना भी वहाँ धूमिल हो रही है, लेकिन वहाँ से उपजे अभिनवगुप्त और उनके सिद्धान्त अब भी अक्षुण्ण हैं। यह दुस्संयोग ही है कि प्रस्तुत पत्र में चर्चा के विषय पाणिनि तथा अभिनव दोनों ही अपनी ज़मीन पर अपदस्थ हो चुके हैं। वहाँ उनको समझने की बात छोड़ दें उनका नामलेवा कोई नहीं रहा। लेकिन फिर भी, राजनैतिक कुचक्र सरस्वतीपुत्रों के माहात्म्य को ऐकान्तिक रूप से समाप्त नहीं कर पाये हैं।
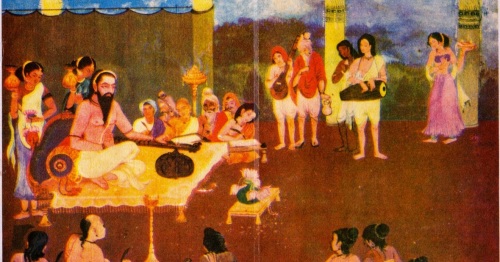
अभिनवगुप्त शैवदर्शन, तन्त्र तथा काव्यशास्त्र की परम्परा के अपूर्व व्याख्याकार हैं। वे सुदीर्घ कालावधि में फैली चिन्तन परम्पराओं को समग्रता में देखकर समेकित रूप में व्याख्या करते हैं, इसलिए उनके दर्शन एवं तन्त्र से सम्बद्ध ग्रन्थ, टीकाग्रन्थ व स्तोत्र तथा फुटकर काव्य आदि मिलाकर परम्परा की व्याख्या का महावाक्य बनता है (त्रिपाठी २०१६:४)। अभिनव का जो भी अभिनवत्व है वह उनकी व्याख्या का ही है। उन्होंने व्याख्याओं के द्वारा परम्परा को जो योगदान दिया वह मूल ग्रन्थों के प्रणयन से कम नहीं है। उन्होंने अपनी व्याख्याओं से कश्मीर के त्रिक दर्शन को एक समन्वित रूप दिया, नाट्यशास्त्र की महावाक्यात्मक कृति के रूप में सप्रमाण विवेचना प्रस्तुत की (त्रिपाठी २०१६:७), ध्वनि तत्त्व को पुनरुज्जीवित किया तथा वैष्णव आधारकारिकाओं का शैवीकृत रूप परमार्थसार भी प्रस्तुत किया[3]।
अपने विशिष्ट व्याख्यान प्रकार में अभिनव ने व्याकरण शास्त्र का अद्भुत तथा अपूर्व उपयोग किया है। व्याकरणशास्त्र सामान्यतः सभी शास्त्रों का उपकारक है इसलिए कोई भी व्याख्या व्याकरण की सहायता के बिना असम्भव है। लेकिन अभिनव के व्याख्या ग्रन्थों में हम व्याकरण शास्त्र की कोटियों का असाधारण उपयोग पाते हैं। प्रकृति तथा प्रत्यय के ज्ञान से शब्द के बाह्य स्वरूप की वास्तविक पहचान हो पाती है तथा इसी कारण किसी भी ग्रन्थ की गुत्थियाँ सुलझाने के लिए टीकाकार व्याकरण की सहायता लेते हैं। लेकिन व्याकरणशास्त्र का उपयोग अभिनव व्याख्येय ग्रन्थ के केवल बाह्य शब्द स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए नहीं करते बल्कि इसका प्रयोग वह अपनी दार्शनिक मान्यताओं के प्रतिपादन तथा स्पष्टीकरण में भी करते हैं। व्याकरण शास्त्र के इस विशिष्ट उपयोग से अभिनव का सम्पूर्ण व्याकरण तन्त्र पर असाधारण अधिकार द्योतित होता है।
अभिनव व्युत्पत्त्यै सर्वशिष्यता[4] तथा बहुभिर्बहु बोद्धव्यं[5] के मूर्तिमान् उदाहरण थे। ज्ञान के प्रति अपनी प्रगाढ पिपासा के चलते अभिनव ने प्रायः सभी शास्त्रों का अध्ययन उस समय के विद्वानों के पास जाकर किया था। परन्तु व्याकरण शास्त्र तो उनके घर की विद्या थी। व्याकरण के उनके गुरु स्वयं उनके पिता नरसिंह गुप्त (चखुल अथवा चुखुलक) थे जिनसे उन्होंने महाभाष्य का अध्ययन किया था। कश्मीर में पाणिनीय व्याकरण, विशेषतः महाभाष्य के अध्ययन की समृद्ध परम्परा रही है। व्याख्यान के क्रम में अभिनव में नूतन आयामों को प्रकट करने की जो क्षमता दिखायी पड़ती है, उसमें महाभाष्यकार पतञ्जलि का बहुत बड़ा योगदान देखा जा सकता है। उनके नाम के विषय में परम्परा में जो व्याख्यायें मिलती हैं उसमें एक के अनुसार उन्हें महाभाष्यकार पतञ्जलि का अवतार बताया जाता है। अभिनवगुप्तपाद शब्द में गुप्तपाद का अर्थ सर्प अथवा शेषनाग है। इस प्रकार इनके नाम का अर्थ होगा– शेषनाग अर्थात् पतञ्जलि के नवीन अवतार[6]। इस व्याख्या से पता चलता है कि उस समय उनकी प्रसिद्धि एक प्रख्यात वैयाकरण के रूप में थी। जब हम उनके ग्रन्थों का अध्ययन करते हैं तो पदे पदे उनके व्याकरण ज्ञान तथा उसके अपूर्व उपयोग से चकित रह जाते हैं। आगे के पृष्ठों में हम उनके व्याकरण ज्ञान के तत्त्वशास्त्रीय उपयोग के कुछ प्रमुख बिन्दुओं की ओर ध्यान आकृष्ट करेंगे।
अभिनवगुप्त व्याकरण के प्रक्रिया तथा दर्शन दोनों पक्षों से सुपरिचित थे तथा उन्होंने दोनों का अपनी व्याख्याओं में यथास्थान उपयोग किया। व्याख्येय ग्रन्थों के सम्प्रत्ययात्मक बीजशब्दों के दार्शनिक तात्पर्य को स्पष्ट करने के लिए वे उन शब्दों की व्युत्पतियाँ प्रस्तुत करते हैं। सामान्यतः, वे व्याकरण शास्त्र की प्रविधियों का उपयोग करते हुए एक शब्द की अनेकानेक व्युत्पत्तियाँ देते हैं। प्रत्येक व्युत्पत्ति से उनका तात्पर्य उस सम्प्रत्यय विशेष के किसी नये आयाम को सुस्पष्ट करना होता है।

0 Comments